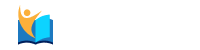Now Reading: श्रीमद् भागवत महापुराण (स्कन्ध 5) | Shrimad Bhagavatam Hindi
- 01
श्रीमद् भागवत महापुराण (स्कन्ध 5) | Shrimad Bhagavatam Hindi
श्रीमद् भागवत महापुराण (स्कन्ध 5) | Shrimad Bhagavatam Hindi
अध्याय 5: भगवान् ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश
संक्षेप विवरण: इस अध्याय में भागवत-धर्म का वर्णन किया गया है, जो भौतिक संताप से मुक्ति दिलानेवाले धार्मिक आदेशों से भी परे हैं। इसमें यह बताया गया है कि मनुष्य को इन्द्रियतृप्ति…
श्लोक 1: भगवान् ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा—हे पुत्रो, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है उसे इन्द्रियतृप्ति के लिए ही दिन-रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कूकर-सूकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगाये। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है, तो उसे शाश्वत जीवन का आनन्द मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत चलने वाला है।
श्लोक 2: आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भव-बन्धन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। ये महापुरुष निर्विशेषवादी तथा भक्त होते हैं। ईश्वर से तदाकार होने अथवा भगवान् का संग प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक मनुष्य को महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। ऐसे कर्मों में रुचि न रखने वाले लोग, जो स्त्री तथा मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं उनके लिए नरक का द्वार खुला रहता है। महात्मा समभाव वाले होते हैं। वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अन्तर नहीं देखते। वे अत्यन्त शान्त होते हैं और भक्ति में पूर्णतया लीन रहते हैं। वे क्रोधरहित होते हैं और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वे कोई निंद्य आचरण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं।
श्लोक 3: जो लोग कृष्णचेतना को पुनरुज्जीवित करने तथा अपना ईश्वर-प्रेम बढ़ाने के इच्छुक हैं, वे ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो श्रीकृष्ण से सम्बन्धित न हो। वे उन लोगों से मेलजोल नहीं बढ़ाते जो अपने शरीर-पालन, भोजन, शयन, मैथुन तथा स्वरक्षा में व्यस्त रहते हैं। वे गृहस्थ होते हुए भी अपने घरबार के प्रति आसक्त नहीं होते। वे पत्नी, सन्तान, मित्र अथवा धन में भी आसक्त नहीं होते, किन्तु उसके साथ ही वे अपने कर्तव्यों के प्रति अन्यमनस्क नहीं रहते। ऐसे पुरुष अपने जीवन-निर्वाह के लिए जितना धन चाहिए उतना ही संग्रह करते हैं।
श्लोक 4: जब मनुष्य इन्द्रियतृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है, तो वह भौतिक रहन-सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पापकर्मों में प्रवृत्त होता है। वह नहीं जानता कि अपने विगत पापकर्मों के ही कारण उसे यह क्षणभंगुर शरीर प्राप्त हुआ है, जो दुखों की खान है। वास्तव में जीवात्मा को भौतिक देह नहीं मिलनी चाहिए थी, किन्तु इन्द्रियतृप्ति के लिए ऐसा हुआ है। अत: मैं मानता हूँ कि बुद्धिमान प्राणी के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह पुन: इन्द्रियतृप्ति के कार्यों में प्रवृत्त हो, जिससे एक के बाद दूसरा शरीर उसे प्राप्त होता रहता है।
श्लोक 5: जब तक जीव को आत्म-तत्त्व की जिज्ञासा नहीं होती तब तक उसे अज्ञानजन्य कष्ट भोगने पड़ते हैं और उसकी पराजय होती रहती है। कर्म का फल पाप अथवा पुण्य कुछ भी हो सकता है। यदि मनुष्य किसी कर्म में व्यस्त रहता है, तो उसका मन सकाम कर्म में रँगा हुआ कहा जाता है। जब तक मन अशुद्ध रहता है, चेतना अस्पष्ट रहती है और जब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा रहता है, तब तक उसे देह धारण करनी पड़ती है।
श्लोक 6: जब जीवात्मा तमोगुण से आच्छादित रहता है, तो वह न तो आत्मा को और न परम-आत्मा को समझता है और उसका मन सकाम कर्म के वशीभूत रहता है। अत: जब तक उसकी मुझ वासुदेव में प्रीति नहीं होती, तब तक उसे देह-बन्धन को स्वीकार करने से छुटकारा नहीं मिल पाता।
श्लोक 7: भले कोई कितना ही विद्वान तथा चतुर क्यों न हो, यदि वह यह नहीं समझ पाता कि इन्द्रियतृप्ति के लिए की जाने वाली चेष्टाएँ व्यर्थ ही समय की बरबादी है, तो वह पागल है। वह आत्म-हित को भूलकर इस संसार में विषयवासना-प्रधान तथा समस्त भौतिक क्लेशों के आगार अपने घर में आसक्त रहकर प्रसन्न रहना चाहता है। इस प्रकार मनुष्य मूर्ख पशु के ही तुल्य होता है।
श्लोक 8: स्त्री तथा पुरुष के मध्य का आकर्षण भौतिक अस्तित्व का मूल नियम है। इस भ्रांत धारणा के कारण स्त्री तथा पुरुष के हृदय परस्पर जुड़े रहते हैं। इसी के फलस्वरूप मनुष्य अपने शरीर, घर, सन्तान, स्वजन तथा धन के प्रति आकृष्ट होता है। इस प्रकार वह जीवन के मोहों को बढ़ाता है और “मैं तथा मेरा” के रूप में सोचता है।
श्लोक 9: जब पूर्व कर्म-फलों के कारण भौतिक जीवन में फँसे हुए व्यक्ति के हृदय की मजबूत गाँठ ढीली पड़ जाती है, तो वह घर, स्त्री तथा सन्तान के प्रति अपनी आसक्ति से विमुख होने लगता है। इस तरह उसका मोह (मैं तथा मेरा) टूट जाता है, वह मुक्त हो जाता है और उसे दिव्य लोक की प्राप्ति होती है।
श्लोक 10-13: हे पुत्रो, तुम्हें सिद्ध गुरु अर्थात् परमहंस को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार तुम मुझ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान् पर अपनी श्रद्धा तथा प्रेम रखो। तुम्हें इन्द्रियतृप्ति से घृणा करनी चाहिए तथा ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के समान आनन्द तथा पीड़ा की द्वैतता को सहना चाहिए। उन जीवात्माओं की कष्टमय दशा को समझने का प्रयास करो, जो स्वर्ग में भी दुखी रहती हैं। सत्य का दार्शनिक तौर पर अन्वेषण करो। फिर भक्ति के निमित्त समस्त प्रकार की तपस्या करो। इन्द्रिय-सुख के लिए प्रयत्नों का परित्याग करके ईश्वर की सेवा में लगो। भगवान् की कथा का श्रवण करो और सदैव भक्तों की संगति करो। ईश्वर का कीर्तन और गुणगान करो और सबों को आध्यात्मिक स्तर पर समभाव से देखो। शत्रुता त्याग कर क्रोध तथा शोक का दमन करो। स्वयं को देह तथा घर के साथ न जोड़ते हुए शास्त्रों का अध्ययन करो। एकान्त वास करो और प्राणवायु (श्वास), मन तथा इन्द्रियों को पूर्णतया वश में करने का अभ्यास करो। वैदिक साहित्य अर्थात् शास्त्रों पर पूर्ण श्रद्धा रखो और सदैव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। अपने कर्तव्यों को करते हुए व्यर्थ की बातें करने से बचो। सदैव भगवान् का चिन्तन करते हुए सही स्रोत से ज्ञान प्राप्त करो। इस प्रकार उत्साह एवं धैर्यपूर्वक भक्तियोग का अभ्यास करते रहने से तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा और अहंकार जाता रहेगा।
श्लोक 14: हे पुत्रो, तुम्हें मेरे उपदेश के अनुसार आचरण करना चाहिए। अत्यन्त सावधान रहना। इन विधियों से तुम लोग सकर्म-अभिलाषा की अविद्या से छूट सकोगे और तुम्हारे हृदय में स्थित बन्धनरूपी ग्रंथि पूर्णतया कट जाएगी। तदनन्तर और अधिक उन्नति के लिए तुम्हें साधनों का परित्याग कर देना चाहिए, अर्थात् तुम्हें मुक्ति-क्रिया में ही आसक्त नहीं हो जाना चाहिए।
श्लोक 15: यदि किसी मनुष्य को घर लौटने अर्थात् ईश्वर के धाम वापस जाने की अभिलाषा हो, तो उसे चाहिए कि वह भगवान् के अनुग्रह को जीवन का परम लक्ष्य माने। यदि वह पिता है, तो अपने पुत्रों को, यदि गुरु है, तो अपने शिष्यों को और यदि राजा है, तो अपनी प्रजा को, इसी प्रकार शिक्षा दे जैसा कि मैंने उपदेश दिया है। उसे चाहिए कि क्रोधरहित होकर इन्हें शिक्षा देते रहें, भले ही शिष्य, पुत्र अथवा प्रजा उनकी आज्ञा का पालन करने में कभी-कभी असमर्थ क्यों न रहें। कर्म-मूढों को जो पाप एवं पुण्य कर्मों में लगे रहते हैं, चाहिए कि वे सभी प्रकार से भक्ति में लगें। उन्हें सकाम कर्म से सदैव बचना चाहिए। यदि शिष्य, पुत्र या प्रजा, जो दिव्य दृष्टि से रहित हो, उसे कर्म के बन्धन में डाला जाये तो भला वह कैसे लाभान्वित होगा? यह अंधे मनुष्य को अंधेरे कुएं तक ले जाने और उसे गिरने देने जैसा है।
श्लोक 16: अज्ञानवश भौतिकतावादी व्यक्ति अपना सच्चा हित नहीं समझ पाता जो जीवन का कल्याणकारी मार्ग है। वह भौतिक सुख की कामेच्छाओं से बँधा रहता है और उसकी सारी योजनाएँ इसी एक कार्य के लिए तैयार की जाती हैं। ऐसा व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए वैरपूर्ण समाज की सृष्टि करता है और अपनी मानसिकता के कारण वह दुख के सागर में कूद पड़ता है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को इसका ज्ञान भी नहीं होता।
श्लोक 17: यदि कोई अज्ञानी है और संसार-पथ में लिप्त है, तो भला उसे कोई विद्वान, दयालु तथा आत्मज्ञानी पुरुष सकाम कर्म करने तथा भौतिक संसार में और अधिक फँसने के लिए क्योंकर प्रवृत्त करेगा? यदि कोई अन्धा व्यक्ति उल्टी राह पर जा रहा हो, तो ऐसा कौन-सा सज्जन पुरुष होगा, जो उसे संकट के पथ पर और आगे जाने देगा? वह इस विधि को क्यों सही मानने लगा? कोई भी बुद्धिमान अथवा दयालु व्यक्ति ऐसा नहीं होने देगा।
श्लोक 18: “जो अपने आश्रित को बारम्बार के जन्म-मृत्यु के पथ से न उबार सके उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माँ या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए।”
श्लोक 19: मेरा दिव्य शरीर (सच्चिदाननन्द विग्रह) मानव सदृश दिखता है, किन्तु यह भौतिक मनुष्य शरीर नहीं है। यह अकल्पनीय है। मुझे प्रकृति द्वारा बाध्य होकर किसी विशेष प्रकार का शरीर नहीं धारण करना पड़ता, मैं अपनी इच्छानुकूल शरीर धारण करता हूँ। मेरा हृदय भी दिव्य है और मैं सदैव अपने भक्तों का कल्याण चाहता रहता हूँ। इसलिए मेरे हृदय में भक्ति पूरित है, जो भक्तों के लिए है। मैंने अधर्म को हृदय से बहुत दूर भगा दिया है। मुझे अभक्ति के कार्य बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इन दिव्य गुणों के कारण सामान्य रूप से लोग मेरी उपासना भगवान् ऋषभदेव के रूप में करते हैं, जो भी जीवात्माओं में श्रेष्ठ है।
श्लोक 20: मेरे प्रिय पुत्रो, तुम सभी मेरे हृदय से उत्पन्न हो जो समस्त दिव्य गुणों का केन्द्र है। अत: तुम्हें संसारी तथा ईर्ष्यालु मनुष्यों के समान नहीं होना है। तुम अपने सबसे बड़े भाई भरत को मानो, क्योंकि वह भक्ति में श्रेष्ठ है। यदि तुम लोग भरत की सेवा करोगे तो उसकी सेवा में मेरी सेवा सम्मिलित होगी और तुम स्वयमेव प्रजा पर शासन करोगे।
श्लोक 21-22: दो प्रकार की प्रकट शक्तियों (आत्मा तथा जड़ पदार्थ) में से जीव-शक्ति (वनस्पति, घास, वृक्ष तथा पौधे) जड़ पदार्थ (पत्थर, पृथ्वी इत्यादि) से श्रेष्ठ है। इन अचर पौधों तथा वनस्पतियों की तुलना में रेंगने वाले कीट तथा सरीसृप श्रेष्ठ हैं। कीटों तथा सरीसृपों से पशु श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनमें बुद्धि है। पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ हैं और मनुष्यों से भूत-प्रेत क्योंकि उनके कोई भौतिक शरीर नहीं होता। भूत-प्रेतों से गंधर्व और गंधर्वों से सिद्ध श्रेष्ठ होते हैं। सिद्धों से किन्नर और किन्नरों से असुर श्रेष्ठ हैं। असुरों से देवता और देवताओं में स्वर्ग का राजा इन्द्र श्रेष्ठ है। इन्द्र से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र, जैसे कि राजा दक्ष और ब्रह्मा के इन पुत्रों में भगवान् शिव सर्वश्रेष्ठ हैं। शिव ब्रह्मा के पुत्र हैं इसलिए ब्रह्मा श्रेष्ठ माने जाते हैं किन्तु वे मुझ भगवान् के अधीन हैं। चूँकि मैं ब्राह्मणों को पूज्य मानता हूँ इसलिए ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं।
श्लोक 23: हे पूज्य ब्राह्मणो, जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, इस संसार में ब्राह्मणों के तुल्य या उनसे श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। मैं उनके तुलना योग्य किसी को नहीं पाता। वैदिक नियमों के अनुसार यज्ञ करने के पीछे जो मेरा उद्देश्य है, उसे जब लोग समझ लेते हैं, तो वे मेरे निमित्त अर्पित भोग अत्यन्त श्रद्धा तथा प्रेमपूर्वक ब्राह्मण-मुख के द्वारा मुझे प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रदत्त भोजन को मैं अत्यन्त प्रसन्न होकर ग्रहण करता हूँ। निस्संदेह इस प्रकार से प्रदत्त भोजन को मैं अग्निहोत्र में होम किये भोजन की अपेक्षा अधिक प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करता हूँ।
श्लोक 24: वेद मेरे शाश्वत दिव्य शब्दावतार हैं, इसलिए वे शब्द-ब्रह्म हैं। इस जगत में ब्राह्मण समस्त वेदों का सम्यक् अध्ययन करते हैं और उनको आत्मसात् कर लेते हैं, इसलिए उन्हें साक्षात् मूर्तरूप वेद माना जाता है। ब्राह्मण सतोगुणी होते हैं फलस्वरूप उनमें शम, दम एवं सत्य के गुण पाये जाते हैं। वे वेदों का मूल अर्थ वर्णन करते हैं और अनुग्रहवश समस्त बद्धजीवों को वेदों के उद्देश्य का उपदेश देते हैं। वे तपस्या तथा तितिक्षा का अभ्यास करते हैं और जीवात्मा तथा परम ईश्वर के पदों का अनुभव करते हैं। ये ही ब्राह्मणों के आठ गुण (सत्त्व, शम, दम, सत्य, अनुग्रह, तपस्या, तितिक्षा यथा अनुभव) हैं। अत: समस्त जीवों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं।
श्लोक 25: मैं ब्रह्मा तथा स्वर्ग के राजा इन्द्र से भी अधिक ऐश्वर्यवान, सर्वशक्तिमान तथा श्रेष्ठ हूँ। मैं स्वर्गलोक में प्राप्त होने वाले समस्त सुखों को तथा मोक्ष को देने वाला हूँ। तो भी ब्राह्मण मुझसे भौतिक सुख की कामना नहीं करते। वे अत्यन्त पवित्र तथा निस्पृह हैं। वे एकमात्र मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। भला उन्हें अन्य किसी से भौतिक लाभों के लिए याचना करने की क्या आवश्यकता है?
श्लोक 26: हे पुत्रो, तुम्हें चराचर किसी जीवात्मा से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यह जानते हुए कि मैं उनमें स्थित हूँ, प्रत्येक क्षण उनका समादर करना चाहिए। इस प्रकार तुम मेरा आदर करो।
श्लोक 27: मन, दृष्टि, वचन तथा समस्त ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय इन्द्रियों का वास्तविक कार्य मेरी सेवा में लगे रहना है। जब तक जीवात्मा की इन्द्रियाँ इस प्रकार सेवारत नहीं रहतीं, तब तक जीवात्मा को यमराज के पाश सदृश सांसारिक बन्धन से निकल पाना दुष्कर है।
श्लोक 28: शुकदेव गोस्वामी ने कहा—इस प्रकार सबके हितैषी परमेश्वर ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया। यह आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कि गृहस्थ जीवन से विरक्त होने के पूर्व पिता अपने पुत्रों को किस प्रकार शिक्षा दे, उन्होंने उन्हें शिक्षा दी, यद्यपि वे सभी पूर्णतया शिक्षित तथा शिष्ट थे। इन उपदेशों से सकाम कर्मों से न बँधने वाले तथा अपनी भौतिक कामनाओं को नष्ट करने के बाद भक्ति में लीन रहने वाले संन्यासी भी लाभ उठाते हैं। ऋषभदेव ने अपने एक सौ पुत्रों को शिक्षा दी जिनमें से सबसे बड़ा भरत था, जो परम भक्त तथा वैष्णवों का अनुयायी था। भगवान् ऋषभदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को सिंहासन पर इसलिए बिठाया कि वह सारे संसार पर शासन करे। इसके पश्चात् घर में रहते हुए भी भगवान् ऋषभदेव पागल के सदृश नंगे तथा बाल बिखेरे रहने लगे। तब यज्ञ-अग्नि को अपने में लीन करके विश्व का भ्रमण करने के लिए उन्होंने ब्रह्मावर्त को छोड़ दिया।
श्लोक 29: अवधूत रूप धारण करके भगवान् ऋषभदेव अंधे, बहरे तथा गूँगे, जड़, भूत अथवा पागल के समान मनुष्य-समाज में घूमने लगे। यद्यपि लोग उन्हें इन नामों से पुकारते, किन्तु वे मूक बने रहते और किसी से कुछ नहीं बोलते थे।
श्लोक 30: ऋषभदेव नगरों, गाँवों, खानों, किसानों की बस्तियों, घाटियों, बागों, सैनिक छावनियों, गोशालाओं, अहीरों की बस्तियों, यात्रियों के विश्रामालयों, पर्वतों, जंगलों तथा आश्रमों के बीच घूमने लगे। जहाँ भी वे जाते, उन्हें दुष्ट जन उसी प्रकार घेर लेते जिस प्रकार जंगली हाथी को मक्खियाँ घेर लेती हैं। उन्हें डराया धमकाया और मारा जाता, उन पर पेशाब किया जाता और थूका जाता। यहाँ तक कि कभी-कभी उन पर पत्थर, विष्ठा और धूल फेंकी जाती और कभी-कभी तो लोग उनके समक्ष अपानवायु निकालते। इस प्रकार लोग उन्हें भला-बुरा कहते और अत्यधिक यातना देते, किन्तु उन्होंने कभी भी इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि वे यह समझते थे कि इस शरीर का यही अन्त है। वे आत्म-पद पर स्थित थे और सिद्ध होने से ऐसे भौतिक तिरस्कारों की तनिक भी परवाह नहीं करते थे। अर्थात् उन्हें इसका पूर्ण ज्ञान हो चुका था कि पदार्थ (देह) तथा आत्मा पृथक्-पृथक् हैं। उनमें देहात्म-बुद्धि न थी। अत: वे किसी पर क्रुद्ध हुए बिना सारे संसार में अकेले ही घूमने लगे।
श्लोक 31: भगवान् ऋषभदेव के हाथ, पाँव तथा वक्षस्थल अत्यन्त दीर्घ थे। उनके कंधे, मुख तथा अंग-प्रत्यंग अत्यन्त सुगठित तथा सुकोमल थे। उनका मुख उनकी सहज मुस्कान से मंडित था और उनके खुले हुए लाल-लाल नेत्र ऐसे प्रतीत होते थे मानो प्रात:कालीन ओस कणों से युक्त नव विकसितकमल पुष्प की पंखडिय़ाँ हों। इस कारण वे और भी अधिक सुन्दर दिखते थे उनकी पुतलियाँ इतनी मनोहर थीं कि देखने वालों का सारा सन्ताप हर लेती थीं। उनके कपोल, कान, गर्दन, नाक तथा अन्य अंग अतीव सुन्दर थे। उनके मन्द हास से उनका मुख इतना आकर्षक प्रतीत होता था कि विवाहित नारियों का भी मन खिंच जाता था। ऐसा प्रतीत होता था मानो कामदेव ने अपने बाणों से उन्हें बींध दिया हो। उनके सिर के चारों ओर घुँघराली भूरी जटाएँ थीं। उनके सिर के बाल छितरे थे क्योंकि उनका शरीर गंदा और उपेक्षित था। ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्हें किसी भूत ने सता रखा हो।
श्लोक 32: जब भगवान् ऋषभदेव ने देखा कि जनता उनकी योग-साधना में विघ्न रूप है, तो उन्होंने इसकी प्रतिक्रिया में अजगर का सा आचरण (वृत्ति) ग्रहण कर लिया। वे एक ही स्थान पर लेटे रहने लगे। वे लेटे ही लेटे खाते, पीते, पेशाब तथा मल त्याग करते और उसी पर लोट-पोट करते। यहाँ तक कि वे अपने सारे शरीर को अपने ही मल-मूत्र से सान लेते जिससे उनके विरोधी उन्हें विचलित न करें।
श्लोक 33: इस अवस्था में रहने के कारण जनता ने ऋषभदेव को परेशान नहीं किया। परंतु उनके मल- मूत्र से दुर्गन्धि नहीं निकली। उल्टे, उनका मल-मूत्र इतना सुगन्धित था कि अस्सी मील तक का प्रदेश इसकी सुगन्ध से भर गया।
श्लोक 34: इस प्रकार ऋषभदेव ने गायों, हिरणों तथा कौवों की वृत्ति का अनुगमन किया। कभी वे इधर-इधर चलते तो कभी एक स्थान पर बैठे रहते। कभी वे लेट जाते। इस प्रकार वे गाय, हिरण तथा कौवे के समान ही आचरण करते। उन्हीं के समान वे खाते-पीते तथा मल-मूत्र का त्याग करते। इस प्रकार वे लोगों को धोखे में रखे रहे।
श्लोक 35: हे राजा परीक्षित, श्रीकृष्ण के अंश भगवान् ऋषभदेव ने समस्त योगियों को योगसाधना प्रदर्शित करने के उद्देश्य से अनेक विचित्र कार्य किये। वे मुक्ति के स्वामी थे और दिव्य आनन्द में सतत लीन रहते थे। जो हजारों गुणा बढ़ गया था। वसुदेव के पुत्ररुप वासुदेव कृष्ण उनके आदि कारण हैं। उनके स्वरूप में कोई अन्तर नहीं; फलत: भगवान् ऋषभदेव रोने, हँसने तथा थरथराने के प्रिय लक्षण प्रकट करने लगे। वे दिव्य प्रेम में सदैव निमग्न रहते। फलस्वरूप सभी योग शक्तियाँ अपने आप उनके पास पहुँचती—यथा मन की गति से आकाश-गमन, प्रकट और अदृश्य होना, अन्यों के शरीर में प्रवेश कर जाना तथा दूरस्थ वस्तुओं को देख पाना। यद्यपि वे इन सबको कर सकने में समर्थ थे, किन्तु उन्होंने इन शक्तियों का प्रयोग नहीं किया।