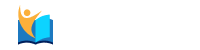Now Reading: श्रीमद् भागवत महापुराण (स्कन्ध 5) | Shrimad Bhagavatam Hindi
- 01
श्रीमद् भागवत महापुराण (स्कन्ध 5) | Shrimad Bhagavatam Hindi
श्रीमद् भागवत महापुराण (स्कन्ध 5) | Shrimad Bhagavatam Hindi
अध्याय 11: जड़ भरत द्वारा राजा रहूगण को शिक्षा
संक्षेप विवरण: इस अध्याय में ब्राह्मण जड़ भरत द्वारा रहूगण को दी गई शिक्षाएँ विस्तार से दी गई हैं। वे राजा से कहते हैं, “आप अधिक अनुभवी नहीं हैं, तो भी आप विद्वान होने का दिखावा…
श्लोक 1: ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा—“हे राजन्, यद्यपि तुम थोड़ा भी अनुभवी नहीं हो तो भी तुम अत्यन्त अनुभवी व्यक्ति के समान बोलने का प्रयत्न कर रहे हो। अत: तुम्हें अनुभवी व्यक्ति नहीं माना जा सकता। अनुभवी व्यक्ति कभी भी तुम्हारे समान स्वामी तथा सेवक अथवा भौतिक सुखों और दुखों के सम्बन्ध में इस प्रकार से नहीं बोलता। ये तो मात्र बाह्य कार्य हैं। कोई भी महान् अनुभवी व्यक्ति परम सत्य को जानते हुए इस प्रकार बातें नहीं करता।”
श्लोक 2: हे राजन्, स्वामी तथा सेवक, राजा तथा प्रजा इत्यादि के प्रसंग तो भौतिक विषय हैं। वेदों में प्रतिपादित भौतिक विषयों में रुचि रखने वाले व्यक्ति यज्ञों को करके तथा भौतिक विषयों के प्रति श्रद्धालु बने रहने पर तुले रहते हैं। ऐसे लोगों को कभी आत्म-तत्त्व प्रकट नहीं हो पाता।
श्लोक 3: स्वप्न मनुष्य को स्वत: झूठा और व्यर्थ लगने लगता है। इसी प्रकार उसे इस लोक में अथवा स्वर्ग में, इसी जीवन में अथवा अगले जन्म में, भौतिक सुख की कामना तुच्छ प्रतीत होने लगती है। जब उसे इसका बोध हो जाता है, तो श्रेष्ठ साधन होने पर भी वेद सत्य का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने में अपर्याप्त लगने लगते हैं।
श्लोक 4: जब तक जीवात्मा का मन तीन गुणों (सतो, रजो तथा तमोगुणों) से दूषित रहता है, तब तक वह स्वच्छन्द, अनियंत्रित हाथी के समान रहता है। वह इन्द्रियों का उपयोग करके शुभ तथा अशुभ कर्मों के क्षेत्र को केवल बृहत्तर बनाता है। परिणाम यह निकलता है कि जीवात्मा इस संसार में भौतिक कर्मों के कारण मात्र सुख तथा दुख का अनुभव करता है।
श्लोक 5: शुभ तथा अशुभ कर्मों की आकांक्षाओं में लीन रहने के कारण मन स्वभावत: काम तथा क्रोध के विकारों से ग्रस्त होता रहता है। इस प्रकार वह भौतिक इन्द्रिय-सुख के प्रति आकृष्ट होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मन सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से संचालित होता है। ग्यारह इन्द्रियों तथा पाँच तत्त्वों—इन सब सोलह कलाओं में से मन प्रधान है। अत: मन के ही कारण विभिन्न देवताओं, मनुष्यों, पशुओं तथा पक्षियों के शरीरों में जन्म लेना पड़ता है। उच्च या निम्न पद पर स्थित होने के अनुसार ही मन उच्च या निम्न भौतिक देह अंगीकार करता है।
श्लोक 6: सांसारिक मन जीव की आत्मा को आच्छादित करके उसे विभिन्न योनियों में ले जाता है। इसे संसृति कहते हैं। मन के ही कारण जीवात्मा को भौतिक दुख तथा सुख का बोध होता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त यह शुभ तथा अशुभ विषयों तथा उनके कर्म को उत्पन्न करता है। इस प्रकार आत्मा बद्ध हो जाता है।
श्लोक 7: मन जीवात्मा को इस संसार में विभिन्न योनियों में फिरता रहता है, जिससे जीवात्मा को मनुष्यों, देवताओं, स्थूल-कृश मनुष्यों इत्यादि विविध रूपों का लौकिक अनुभव होता है। विद्वानों का कथन है कि देह का रूपायन बन्धन तथा मुक्ति का कारण मन ही है।
श्लोक 8: जब जीवात्मा का मन सांसारिक इन्द्रिय-तृप्ति में लीन हो जाता है, तो जीवन-बंधन तथा सांसारिक कष्ट प्राप्त होते हैं। किन्तु जब वह उनसे अनासक्त हो जाता है, तो वही मुक्ति का कारण बनता है। जब दीपक की बत्ती से ठीक-ठीक लौ नहीं उठती तो दीपक पर कालिख लग जाती है। किन्तु घी से भरा होने पर यह ठीक से जलता है और तीव्र प्रकाश निकलता है। इसी प्रकार जब मन इन्द्रिय-तृप्ति में संलग्न रहता है, तो इससे कष्ट प्राप्त होते हैं और जब यह उनसे विरक्त हो जाता है, तो कृष्णभावनामृत का आदि प्रकाश निकलने लगता है।
श्लोक 9: पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ। इनके साथ ही अहंकार भी है। इस प्रकार मन की ग्यारह प्रकार की वृत्तियाँ हैं। हे वीर, इन्द्रियों के विषय (यथा शब्द और स्पर्श), कायिक कर्म (यथा मलत्याग) तथा विभिन्न प्रकार के देह, समाज, मैत्री तथा व्यक्तित्व—इन सबको पण्डित लोग मन के कार्य के अन्तर्गत मानते हैं।
श्लोक 10: शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद (रस) तथा गन्ध—ये पांच ज्ञानेन्द्रियों के व्यापार हैं। भाषण, स्पर्श, संचलन, मलत्याग तथा संभोग—ये कर्मेन्द्रियों के कार्य हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य धारणा है, जिसके अन्तर्गत मनुष्य सोचता है कि, “यह मेरा शरीर है, यह मेरा समाज है, यह मेरा परिवार हैं, यह मेरा राष्ट्र है।” यह ग्यारहवाँ व्यापार मन का है और मिथ्या अहंकार कहलाता है। कुछ दार्शनिकों के अनुसार यह बारहवाँ व्यापार है और इसका कार्यक्षेत्र शरीर है।
श्लोक 11: भौतिक तत्त्व (द्रव्य या विषय), प्रकृति (स्वभाव), मूल कारण, संस्कार, भाग्य तथा समय (काल)—ये सब भौतिक कारण हैं। इन भौतिक कारणों से विक्षुब्ध होकर ग्यारह वृत्तियाँ पहले सैकड़ों, फिर हजारों और तब करोड़ों भेदों में रूपान्तरित हो जाती हैं। किन्तु ये सभी भेद स्वत: परस्पर मिश्रण के द्वारा घटित नहीं होते वरन् वे श्रीभगवान् के आदेशानुसार होते हैं।
श्लोक 12: कृष्णचेतना से रहित जीव के मन में माया द्वारा उत्पन्न अनेक विचार तथा वृत्तियाँ होती हैं। वे अनन्त काल से विद्यमान रही हैं। कभी-कभी वे जाग्रत तथा स्वप्न अवस्था में प्रकट होती हैं, किन्तु सुषुप्तावस्था या समाधि में वे लुप्त हो जाती हैं। जो व्यक्ति इस जन्म में ही मुक्त हो चुका है, (जीवन्मुक्त ) इन सब व्यापारों को स्पष्ट देख सकता है।
श्लोक 13-14: क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के हैं—जीवात्मा तथा श्रीभगवान्। (जीवात्मा का वर्णन पीछे किया जा चुका है, यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान् की विवेचना की जा रही है) श्रीभगवान् सृष्टि का सर्वव्यापक कारण है। वह अपने में पूर्ण है और अन्यों पर आश्रित नहीं है। वह सुनकर तथा प्रत्यक्ष अनुभव (दर्शन) से देखा जाता है। वह आत्मतेजस्वी है और उसे जन्म, मृत्यु, जरा अथवा व्याधि कुछ भी नहीं सताते। वह ब्रह्मादि समस्त देवताओं का नियन्ता है। उसका नाम नारायण है और वह संसार के प्रलय के पश्चात् समस्त जीवात्माओं का आश्रय है। वह परम ऐश्वर्यवान है और समस्त भौतिक वस्तुओं का आश्रय है। अत: वह वासुदेव अर्थात् पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान् के नाम से जाना जाता है। अपनी शक्ति से ही वह समस्त जीवात्माओं के हृदयों में स्थित है, जिस प्रकार समस्त चराचर प्राणियों में वायु या जीवनीशक्ति (प्राण) रहती है। इस प्रकार वह शरीर को वश में रखता है। अपने अंश रूप में श्रीभगवान् समस्त देहों में प्रवेश करके उनको नियंत्रित करता रहता है।
श्लोक 15: हे राजा रहूगण, जब तक बद्ध-आत्मा भौतिक देह को स्वीकार करता है और भौतिक सुख के कल्मष से मुक्त नहीं हो जाता तथा जब तक अपने छ: शत्रुओं को जीत कर आत्मज्ञान को जागृत करके आत्म-साक्षात्कार के पद को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उसे इस जगत में विभिन्न स्थानों तथा नाना योनियों में घूमना पड़ता है।
श्लोक 16: इस संसार में आत्मा की उपाधि, यह मन, समस्त दुखों का मूल है। जब तक बद्ध जीवात्मा इस तथ्य को नहीं जानता, तब तक उसे देह की दयनीय दशा को स्वीकार करके इस ब्रह्माण्ड में विभिन्न योनियों में घूमना पड़ता है। चूँकि यह मन रोग, शोक, मोह, राग, लोभ तथा वैर से ग्रस्त रहता है इस कारण से इस भौतिक संसार में बन्धन तथा झूठी ममता उत्पन्न होती है।
श्लोक 17: यह अनियंत्रित मन जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि इसकी उपेक्षा की जाती है या इसे अवसर प्रदान किया जाता हैं, तो यह प्रबल से प्रबलतर होकर विजयी बन सकता है। यद्यपि यह यथार्थ नहीं है, किन्तु यह अत्यधिक प्रबल होता है। यह आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को आच्छादित कर देता है। हे राजन्, इस मन को गुरु के चरणारविन्द तथा भगवान् की सेवा रूपी अस्त्र से जीतने का प्रयत्न कीजिये। इसे अत्यन्त सतर्कता से करें।