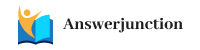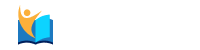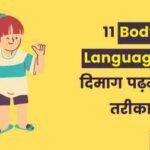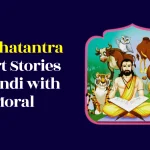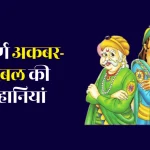Now Reading: श्रीमद् भागवत महापुराण (स्कन्ध 5) | Shrimad Bhagavatam Hindi
- 01
श्रीमद् भागवत महापुराण (स्कन्ध 5) | Shrimad Bhagavatam Hindi
श्रीमद् भागवत महापुराण (स्कन्ध 5) | Shrimad Bhagavatam Hindi
अध्याय 10: जड़ भरत तथा महाराज रहूगण की वार्ता
संक्षेप विवरण: इस अध्याय में भरत महाराज अर्थात् जड़ भरत को सिंधु तथा सौवीर राज्यों के शासक राजा रहूगण ने अंगीकार कर लिया। उस राजा ने जड़ भरत को अपनी पालकी ढोने के लिए विवश किया…
श्लोक 1: शुकदेव गोस्वामी आगे बोले, हे राजन्, इसके बाद सिंधु तथा सौवीर प्रदेशों का शासक रहूगण कपिलाश्रम जा रहा था। जब राजा के मुख्य कहार (पालकीवाहक) इक्षुमती के तट पर पहुँचे तो उन्हें एक और कहार की आवश्यकता हुई। अत: वे किसी ऐसे व्यक्ति की खोज करने लगे और दैववश उन्हें जड़ भरत मिल गया। उन्होंने सोचा कि यह तरुण और बलिष्ठ है और इसके अंग-प्रत्यंग सुदृढ़ हैं। यह बैलों तथा गधों के तुल्य बोझा ढोने के लिए अत्यन्त उपयुक्त है। ऐसा सोचते हुए यद्यपि महात्मा जड़ भरत ऐसे कार्य के लिए सर्वथा अनुपयुक्त थे तो भी कहारों ने बिना झिझक के पालकी ढोने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया।
श्लोक 2: किन्तु अपने अहिंसक भाव के कारण जड़ भरत पालकी को ठीक से नहीं ले जा रहे थे। जैसे ही वे आगे बढ़ते, हर तीन फुट पहले वे यह देखने के लिए रुक जाते कि कहीं कोई चींटी पर पांव तो नहीं पड़ रहा है। फलत: वे अन्य कहारों से ताल-मेल नहीं बैठा पा रहे थे। इसके कारण पालकी हिल रही थी। अत: राजा रहूगण ने तुरन्त कहारों से पूछा, “तुम लोग इस पालकी को ऊँची-नीची करके क्यों लिए जा रहे हो? अच्छा हो, यदि उसे ठीक से ले चलो।”
श्लोक 3: जब कहारों ने महाराजा रहूगण की धमकी सुनी तो वे उसके दण्ड से अत्यन्त भयभीत हो गये और उनसे इस प्रकार कहने लगे।
श्लोक 4: हे स्वामी, कृपया ध्यान दें कि हम अपना कार्य करने में तनिक भी असावधान नहीं हैं। हम इस पालकी को आपकी इच्छानुसार निष्ठा से ले जा रहे हैं, किन्तु यह व्यक्ति, जिसे हाल ही में काम में लगाया गया है, तेजी से नहीं चल पा रहा। अत: हम उसके साथ पालकी ले जाने में असमर्थ हैं।
श्लोक 5: राजा रहूगण दण्ड से भयभीत कहारों के वचन का अभिप्राय समझ रहा था। उसकी समझ में यह भी आ गया कि मात्र एक व्यक्ति के दोष के कारण पालकी ठीक से नहीं चल रही। यह सब अच्छी प्रकार जानते हुए तथा उनकी विनती सुनकर वह कुछ-कुछ क्रुद्ध हुआ, यद्यपि वह राजनीति में निपुण एवं अत्यन्त अनुभवी था। उसका यह क्रोध राजा के जन्मजात स्वभाव से उत्पन्न हुआ था। वस्तुत: राजा रहूगण का मन रजोगुण से आवृत था, अत: वह जड़ भरत से, जिनका ब्रह्मतेज राख से ढकी अग्नि के समान सुस्पष्ट नहीं था, इस प्रकार बोला।
श्लोक 6: राजा रहूगण ने जड़ भरत से कहा : मेरे भाई, यह कितना कष्टप्रद है! तुम निश्चित ही अत्यन्त थके लग रहे हो, क्योंकि तुम बहुत समय से और लम्बी दूरी से किसी की सहायता के बिना अकेले ही पालकी ला रहे हो। इसके अतिरिक्त, बुढ़ापे के कारण तुम अत्यधिक परेशान हो। हे मित्र, मैं देख रहा हूँ कि तुम न तो मोटे-ताजे हो, न ही हट्टे-कट्टे हो। क्या तुम्हारे साथ के कहार तुम्हें सहयोग नहीं दे रहे? इस प्रकार राजा ने जड़ भरत को ताना मारा, किन्तु इतने पर भी जड़ भरत को शरीर की सुधि नहीं थी। उसे ज्ञान था कि वह शरीर नहीं है, क्योंकि वह स्वरूपसिद्ध हो चुका था। वह न तो मोटा था, न पतला, न ही उसे पंच स्थूल भूतों तथा तीन सूक्ष्म तत्त्वों के इस स्थूल पदार्थ से कुछ लेना-देना था। उसे भौतिक शरीर तथा इसके दो हाथों तथा दो पैरों से कोई सरोकार न था। दूसरे शब्दों में, कहना चाहें तो कह सकते हैं कि वह ‘अहं ब्रह्मास्मि’ अर्थात् ब्रह्म रूप को प्राप्त हो चुका था। अत: राजा की व्यंग्य पूर्ण आलोचना का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बिना कुछ कहे पूर्ववत् पालकी को उठाये चलता रहा।
श्लोक 7: तत्पश्चात्, जब राजा ने देखा कि उसकी पालकी अब भी पूर्ववत् हिल रही थी, तो वह अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और कहने लगा—अरे दुष्ट ! तू क्या कर रहा है? क्या तू जीवित ही मर गया है? क्या तू नहीं जानता कि मैं तेरा स्वामी हूँ? तू मेरा अनादर कर रहा है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन भी। इस अवज्ञा के लिए मैं अब तुझे मृत्यु के अधीक्षक यमराज के ही समान दण्ड दूँगा। मैं तेरा सही उपचार किये देता हूँ, जिससे तू होश में आ जाएगा और ठीक से काम करेगा।
श्लोक 8: राजा रहूगण अपने को राजा समझने के कारण देहात्मबुद्धि से ग्रस्त था और भौतिक प्रकृति के रजो तथा तमो गुणों से प्रभावित था। दम्भ के कारण उसने जड़ भरत को अशोभनीय वचनों से दुत्कारा। जड़ भरत महान् भक्त और श्रीभगवान् के प्रिय धाम थे। यद्यपि राजा अपने आपको बड़ा विद्वान मानता था, किन्तु वह न तो महान् भक्त की स्थिति से और न उसके गुणों से परिचित था। जड़ भरत तो साक्षात् भगवान् के परम धाम थे और अपने हृदय में ईश्वर के स्वरूप को धारण करते थे। वे समस्त प्राणियों के प्रिय मित्र थे और किसी प्रकार की देहात्म-बुद्धि को नहीं मानते थे। अत: वे मुस्काये और इस प्रकार बोले।
श्लोक 9: महान् ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा—हे राजन् तथा वीर, आपने जो कुछ व्यंग्य में कहा है, वह सचमुच ठीक है। ये मात्र उलाहनापूर्ण शब्द नहीं हैं, क्योंकि शरीर तो वाहक (ढोने वाला) है। शरीर द्वारा ढोया जाने वाला भार मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। आपके कथनों में तनिक भी विरोधाभास नहीं है, क्योंकि मैं शरीर से भिन्न हूँ। मैं पालकी का ढोने वाला नहीं हूँ, वह तो शरीर है। निस्सन्देह, जैसा आपने संकेत किया है, पालकी ढोने में मैंने कोई श्रम नहीं किया है, क्योंकि मैं तो शरीर से पृथक् हूँ। आपने कहा कि मैं हृष्ट-पुष्ट नहीं हूँ। ये शब्द उस व्यक्ति के सर्वथा अनुरूप हैं, जो शरीर तथा आत्मा का अन्तर नहीं जानता। शरीर मोटा या दुबला हो सकता है, किन्तु कोई भी बुद्धिमान यह बात आत्मा के लिए नहीं कहेगा। जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है मैं न तो मोटा हूँ न दुबला। अत: जब आप कहते हैं कि मैं हृष्ट-पुष्ट नहीं हूँ तो आप सही हैं और यदि इस यात्रा का बोझ तथा वहाँ तक जाने का मार्ग मेरे अपने होते तो मेरे लिए अनेक कठिनाइयाँ होतीं, किन्तु इनका सम्बन्ध मुझसे नहीं मेरे शरीर से है, अत: मुझे कोई कष्ट नहीं है।
श्लोक 10: मोटापा, दुबलापन शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, भूख, प्यास, भय, कलह, भौतिक सुख की कामना, बुढ़ापा, निद्रा, भौतिक पदार्थों में आसक्ति, क्रोध, शोक, मोह तथा देहाभिमान—ये सभी आत्मा के भौतिक आवरण के रूपान्तर हैं। जो व्यक्ति देहात्मबुद्धि में लीन रहता है, वही इनसे प्रभावित होता है, किन्तु मैं तो समस्त प्रकार की देहात्मबुद्धि से मुक्त हूँ। फलत: मैं न तो मोटा हूँ, न पतला, न ही वह सब जो आपने मेरे सम्बन्ध में कहा है।
श्लोक 11: हे राजन्, आपने वृथा ही मुझ पर जीवित होने पर भी मृततुल्य होने का आरोप लगाया है। इस भौतिक सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसा सर्वत्र है, क्योंकि प्रत्येक भौतिक वस्तु का अपना आदि तथा अन्त होता है। आपका यह सोचना कि, “मैं राजा तथा स्वामी हूँ” और इस प्रकार आप द्वारा मुझे आज्ञा दिया जाना भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि ये पद अस्थायी हैं। आज आप राजा हैं और मैं आपका दास हूँ, किन्तु कल स्थिति बदल सकती है और आप मेरे दास हो सकते हैं, मैं आपका स्वामी। ये नियति द्वारा उत्पन्न अस्थायी परिस्थितियाँ हैं।
श्लोक 12: हे राजन्, यदि आप अब भी यह सोचते हैं कि आप राजा हैं और मैं आपका दास, तो आप आज्ञा दें और मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना होगा। तो मैं यह कह सकता हूँ कि यह अन्तर क्षणिक है और व्यवहार या परम्परावश प्राप्त होता है। मुझे इसका अन्य कारण नहीं दिखाई पड़ता। उस दशा में कौन स्वामी है और कौन दास? प्रत्येक प्राणी प्रकृति के नियमों द्वारा प्रेरित होता है। अत: न तो कोई स्वामी है, न कोई दास। इतने पर भी यदि आप सोचते हैं कि मैं आपका दास हूँ और आप मेरे स्वामी हैं, तो मैं इसे स्वीकार कर लूँगा। कृपया आज्ञा दें। मैं आपकी क्या सेवा करूँ?
श्लोक 13: हे राजन्, आपने कहा “रे दुष्ट, जड़ तथा पागल! मैं तुम्हारी चिकित्सा करने जा रहा हूँ और तब तुम होश में आ जाओगे।” इस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि यद्यपि मैं जड़, गूँगे तथा बहरे मनुष्य की भाँति रहता हूँ, किन्तु मैं सचमुच एक स्वरूप-सिद्ध व्यक्ति हूँ। आप मुझे दण्डित करके क्या पाएँगे? यदि आपका अनुमान ठीक है और मैं पागल हूँ तो आपका यह दंड एक मरे हुए घोड़े को पीटने जैसा होगा। उससे कोई लाभ नहीं होगा। जब पागल को दंडित किया जाता है, तो उसका पागलपन ठीक नहीं होता है।
श्लोक 14: शुकदेव गोस्वामी ने कहा—हे महाराज परीक्षित, जब राजा रहूगण ने परम भक्त जड़ भरत को अपने कटु वचनों से मर्माहत किया, तो उस शान्त मुनिवर ने सब कुछ सहन कर लिया और समुचित उत्तर दिया। अज्ञानता का कारण देहात्मबुद्धि है, किन्तु जड़ भरत उससे प्रभावित नहीं थे। अपनी स्वाभाविक विनम्रता के कारण उन्होंने अपने को कभी भी महान् भक्त नहीं माना और अपने पूर्व कर्मफल को भोगना स्वीकार किया। सामान्य मनुष्य की भाँति उन्होंने सोचा कि वे पालकी ढोकर अपने पूर्व अपकृत्यों के फल को विनष्ट कर रहे हैं। ऐसा सोचकर वे पूर्ववत् पालकी लेकर चलने लगे।
श्लोक 15: शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा—हे श्रेष्ठ पाण्डुवंशी (महाराज परीक्षित), सिंधु तथा सौवीर के राजा (रहूगण) की परम सत्य की चर्चाओं में श्रद्धा थी। इस प्रकार सुयोग्य होने के कारण, उसने जड़ भरत से वह दार्शनिक उपदेश सुना जिसकी संस्तुति सभी योग साधना के ग्रन्थ करते हैं और जिससे हृदय में पड़ी गाँठ ढीली पड़ती है। इस प्रकार उसका राज-मद नष्ट हो गया। वह तुरन्त पालकी से नीचे उतर आया और जड़ भरत के चरण-कमलों में अपना सिर रखकर पृथ्वी पर दण्डवत् गिर गया जिससे वह इस ब्राह्मण-श्रेष्ठ को कहे गये अपमानपूर्ण शब्दों के लिए क्षमा प्राप्त कर सके। तब उसने इस प्रकार प्रार्थना की।
श्लोक 16: राजा रहूगण बोले, हे ब्राह्मण, आप इस जगत में अत्यन्त प्रच्छन्न भाव से तथा अज्ञात रूप से विचरण करते प्रतीत हो रहे हैं। आप कौन हैं? क्या आप विद्वान ब्राह्मण तथा साधु पुरुष हैं? आपने जनेउ धारण कर रखा है। कहीं आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई विद्वान तो नहीं हैं? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किसके शिष्य हैं? आप कहाँ रहते हैं? आप इस स्थान पर क्यों आये हैं? कहीं आप हमारे कल्याण के लिए तो यहां नहीं आये? कृपया बतायें कि आप कौन हैं?
श्लोक 17: महानुभाव, न तो मुझे इन्द्र के वज्र का भय है, न नागदंश का, न भगवान् शिव के त्रिशूल का। मुझे न तो मृत्यु के अधीक्षक यमराज के दण्ड की परवाह है, न ही मैं अग्नि, तप्त सूर्य, चन्द्रमा, वायु अथवा कुबेर के अस्त्रों से भयभीत हूँ। परन्तु मैं ब्राह्मण के अपमान से डरता हूँ। मुझे इससे बहुत भय लगता है।
श्लोक 18: महाशय, ऐसा प्रतीत होता है कि आपका महत् आध्यात्मिक ज्ञान प्रच्छन्न है। आप समस्त भौतिक संसर्ग से रहित हैं और परमात्मा के विचार में पूर्णतया तल्लीन हैं। इसलिए आपका आध्यात्मिक ज्ञान अनन्त है। कृपया बलताने का कष्ट करें कि आप जड़वत् सर्वत्र क्यों घूम रहे हैं? हे साधु, आपने योगसम्मत शब्द कहे हैं, किन्तु हमारे लिए उनको समझ पाना सम्भव नहीं है। अत: कृपा करके विस्तार से कहें।
श्लोक 19: मैं आपको योग शक्ति का प्रतिष्ठित स्वामी मानता हूँ। आप आत्मज्ञान से भली भाँति परिचित हैं। आप साधुओं में परम पूज्य हैं और आप समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। आप आत्मज्ञान प्रदान करने आये हैं और ईश्वर के अवतार तथा ज्ञान के अंश कपिलदेव के साक्षात् प्रतिनिधि हैं। अत: मैं आपसे पूछ रहा हूँ,“हे गुरु, इस संसार में सर्वाधिक सुरक्षित आश्रय कौन सा है?”
श्लोक 20: क्या यह सच नहीं कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान् के अवतार कपिल देव के साक्षात् प्रतिनिधि हैं? मनुष्यों की परीक्षा लेने और यह देखने के लिए कि वास्तव में कौन मनुष्य है और कौन नहीं, आपने अपने आपको गूँगे तथा बहरे मनुष्य की भाँति प्रस्तुत किया है। क्या आप संसार भर में इसलिए नहीं इस रूप में घूम रहे? मैं तो गृहस्थ जीवन तथा सांसारिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त हूँ और आत्मज्ञान से रहित हूँ। इतने पर भी अब मैं आपसे प्रकाश पाने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप बताएँ कि मैं किस प्रकार आत्मजीवन में प्रगति कर सकता हूँ?
श्लोक 21: आपने कहा कि, “मैं श्रम करने में थकता नहीं हूँ” यद्यपि आत्मा देह से पृथक् है, किन्तु शारीरिक श्रम करने से थकान लगती है और ऐसा लगता है कि यह आत्मा की थकान है। जब आप पालकी ले जा रहे होते हैं, तो निश्चय ही आत्मा को भी कुछ श्रम करना पड़ता होगा। ऐसा मेरा अनुमान है। आपने यह भी कहा है कि स्वामी तथा सेवक का बाह्य आचरण वास्तविक नहीं है, किन्तु प्रत्यक्ष जगत में यह वास्तविकता भले न हो तो भी प्रत्यक्ष जगत पदार्थों से वस्तुएँ प्रभावित तो हो ही सकती हैं। ऐसा दृश्य तथा अनुभवगम्य है। अत: भले ही भौतिक कार्यकलाप अस्थायी हों, किन्तु उन्हें असत्य नहीं कहा जा सकता।
श्लोक 22: राजा रहूगण आगे बोला—महाशय, आपने बताया कि शारीरिक स्थूलता तथा कृशता जैसी उपाधियाँ आत्मा के लक्षण नहीं हैं। यह सही नहीं है, क्योंकि सुख तथा दुख जैसी उपाधियों का अनुभव आत्मा को अवश्य होता है। आप दूध तथा चावल को एक पात्र में भर कर अग्नि के ऊपर रखें तो दूध तथा चावल क्रम से स्वत: तप्त होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक सुखों तथा दुखों से हमारी इन्द्रियाँ, मन तथा आत्मा प्रभावित होते हैं। आत्मा को इस परिवेश से सर्वथा बाहर नहीं रखा जा सकता।
श्लोक 23: महाशय, आपने बताया कि राजा तथा प्रजा अथवा स्वामी और सेवक के सम्बन्ध शाश्वत नहीं होते। यद्यपि ऐसे सम्बन्ध अस्थायी हैं, तो भी जब कोई व्यक्ति राजा बनता है, तो उसका कर्तव्य नागरिकों पर शासन करना और नियमों की अवज्ञा करने वालों को दण्डित करना है। उनको दण्डित करके वह नागरिकों को राज्य के नियमों का पालन करने की शिक्षा देता है। पुन: आपने कहा है कि मूक तथा बधिर को दण्ड देना चर्वित को चर्वण करना या पिसी लुगदी को फिर से पीसना है, जिसका अभिप्राय यह हुआ कि इससे कोई लाभ नहीं होता। किन्तु यदि कोई परमेश्वर द्वारा आदिष्ट अपने कर्तव्यों के पालन में लगा रहता है, तो उसके पापकर्म निश्चय ही घट जाते हैं। अत: यदि किसी को बलपूर्वक उसके कर्तव्यों में लगा दिया जाये तो उसे लाभ पहुँचता है, क्योंकि इस प्रकार उसके समस्त पाप दूर हो सकते हैं।
श्लोक 24: आपने जो भी कहा है उसमें मुझे विरोधाभास लगता है। हे दीनबन्धु, मैंने आपको अपमानित करके बहुत बड़ा अपराध किया है। राजा का शरीर धारण करने के कारण मैं झूठी प्रतिष्ठा से फूला हुआ था, अत: इसके लिए मैं अवश्य ही अपराधी हूँ। अब मेरी प्रार्थना है कि मुझ पर अहैतुक अनुग्रह की दृष्टि डालें। यदि आप ऐसा करें तो आपका अपमान करके मैंने जो पापकर्म किया है उससे मुक्त हो सकूँगा।
श्लोक 25: हे स्वामी, आप समस्त जीवात्माओं के मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान् के सखा हैं। अत: आप सबों के लिए समान हैं और देहात्म-बुद्धि से सर्वथा मुक्त हैं। यद्यपि मैंने आपकी अवमानना करके अपराध किया है, किन्तु मैं जानता हूँ कि मेरे इस तिरस्कार से आपको कोई हानि या लाभ नहीं होने वाला है। आप दृढ़संकल्प हैं जबकि मैं अपराधी हूँ। इसलिए भले ही मैं भगवान् शिव के समान बलवान् क्यों न होऊँ, किन्तु एक वैष्णव के चरणकमल पर अपराध करने के कारण मैं तुरन्त ही नष्ट हो जाऊँगा।